



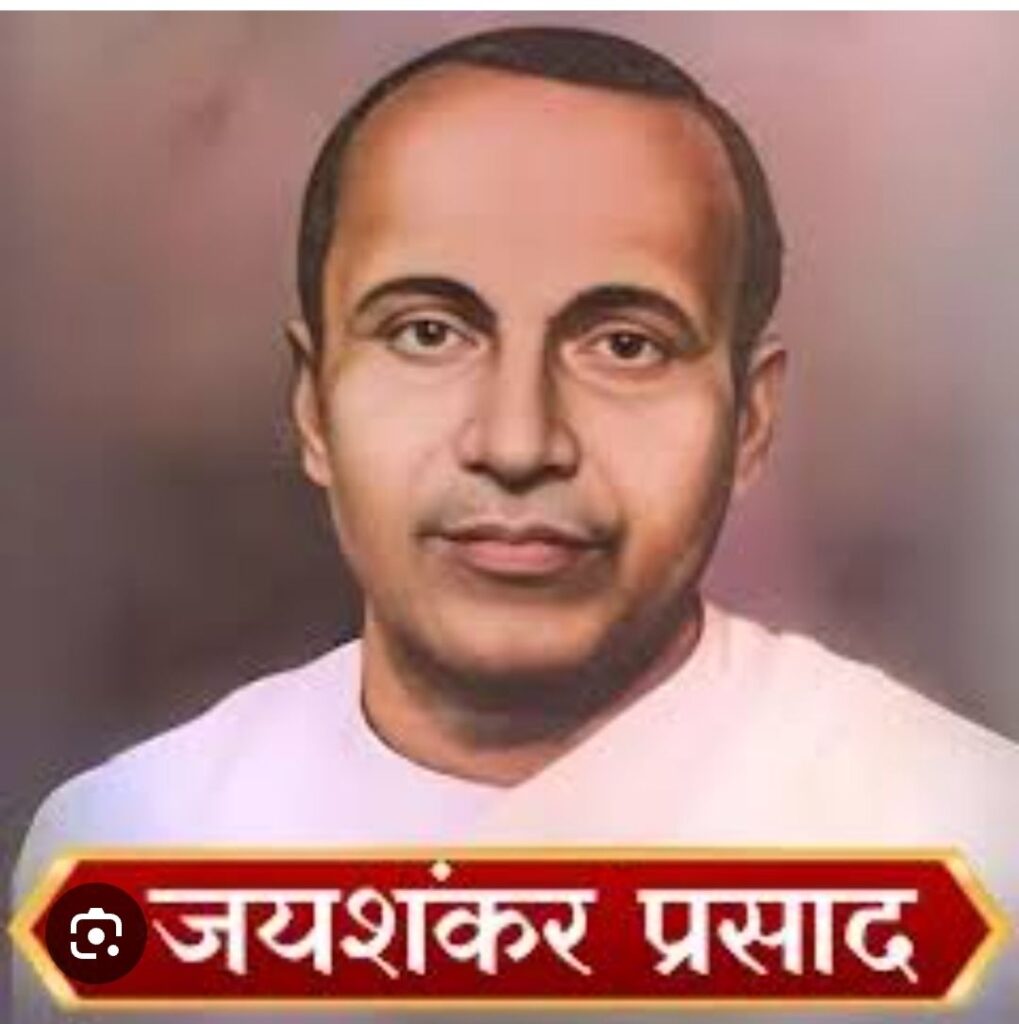
जिस समय खड़ी बोली और आधुनिक हिन्दी साहित्य किशोरावस्था में पदार्पण कर रहे थे उस समय जयशंकर प्रसाद का जन्म सन् 1889 ई. (माघ शुक्ल दशमी, संवत् 1946 वि.) वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कवि के पितामह शिव रत्न साहु वाराणसी के अत्यन्त प्रतिष्ठित नागरिक थे और एक विशेष प्रकार की सुरती (तम्बाकू) बनाने के कारण ‘सुँघनी साहु’ के नाम से विख्यात थे। उनकी दानशीलता सर्वविदित थी और उनके यहाँ विद्वानों कलाकारों का समादर होता था। जयशंकर प्रसाद के पिता देवीप्रसाद साहु ने भी अपने पूर्वजों की परम्परा का पालन किया। इस परिवार की गणना वाराणसी के अतिशय समृद्ध घरानों में थी और धन-वैभव का कोई अभाव न था। प्रसाद का कुटुम्ब शिव का उपासक था। माता-पिता ने उनके जन्म के लिए अपने इष्टदेव से बड़ी प्रार्थना की थी। वैद्यनाथ धाम के झारखण्ड से लेकर उज्जयिनी के महाकाल की आराधना के फलस्वरूप पुत्र जन्म स्वीकार कर लेने के कारण शैशव में जयशंकर प्रसाद को ‘झारखण्डी’ कहकर पुकारा जाता था। वैद्यनाथधाम में ही जयशंकर प्रसाद का नामकरण संस्कार हुआ। जयशंकर प्रसाद की शिक्षा घर पर ही आरम्भ हुई। संस्कृत, हिन्दी, फ़ारसी, उर्दू के लिए शिक्षक नियुक्त थे। इनमें रसमय सिद्ध प्रमुख थे। प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के लिए दीनबन्धु ब्रह्मचारी शिक्षक थे। कुछ समय के बाद स्थानीय क्वीन्स कॉलेज में प्रसाद का नाम लिख दिया गया, पर यहाँ पर वे आठवीं कक्षा तक ही पढ़ सके। प्रसाद एक अध्यवसायी व्यक्ति थे और नियमित रूप से अध्ययन करते थे।
इनके बाल्यकाल में ही इनके पिता जी का देहांत हो गया | किशोरावस्था से पूर्व इनकी माता और बड़े भाई का देहांत हो गया | जिसके कारण 17 वर्ष की उम्र में ही जयशंकर प्रसाद पर अनेक जिम्मेदारियां आ गयी | घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी और परिवार से सम्बद्ध अन्य लोगों ने इनकी सम्पत्ति हड़पने का षड्यंत्र रचा, परिणाम स्वरुप इन्होंने विद्यालय की शिक्षा छोड़ दी और घर में ही अंग्रेजी, हिन्दी, बंगला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्यन किया | ये साहित्यिक प्रवृति के व्यक्ति थे, शिव के उपासक थे और मांस मदिरा से दूर रहते थे | इन्होंने अपने साहित्य साधना से हिन्दी को अनेक उच्चकोटि के ग्रन्थ-रत्न प्रदान किए | इनके गुरुओं में रसमय सिद्ध की भी चर्चा की जाती है | इन्होंने वेद, इतिहास, पुराण व साहित्य का गहन अध्ययन किया था |
सत्रह वर्ष की अवस्था तक इनके माता-पिता एवं ज्येष्ठ भ्राता के देहावसान के कारण गृहस्थी का बोझ आन पड़ा। गृह कलह में साडी समृद्धि जाती रही। इन्ही परिस्थितियों ने प्रसाद के कवि व्यक्तित्व को उभारा। ‘कामायनी’ जैसे महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में अंतर्द्वद्व का जो रूप दिखाई पड़ता है वह इनकी लेखनी का मौलिक गुण है। इनके नाटकों तथा कहानियो में भी यह अंतर्द्वंद्व गहन संवेदना के स्तर पर उपस्थित है। इनकी अधिकांश रचनाएँ इतिहास तथा कल्पना के समन्वय पर आधारित हैं तथा प्रत्येक काल के यथार्थ को गहरे स्तर पर संवेदना की भावभूमि पर प्रस्तुत करती हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में शिल्प के स्तर पर भी मौलिकता के दर्शन होते हैं। उनकी रचनाओं में भाषा की संस्कृतनिष्ठता तथा प्रांजलता विशिष्ट गुण हैं। चित्रात्मक वस्तु-विवरण से संपृक्त उनकी रचनाएँ प्रसाद की अनुभूति और चिंतन के दर्शन कराती हैं।
एक महान लेखक के रूप में प्रख्यात जयशंकर प्रसाद के तितली, कंकाल और इरावती जैसे उपन्यास और आकाशदीप, मधुआ और पुरस्कार जैसी कहानियाँ उनके गद्य लेखन की अपूर्व ऊँचाइयाँ हैं। उनकी कहानियां कविता समान रहती है। काव्य साहित्य में कामायनी बेजोड कृति है । । विविध रचनाओं के माध्यम से मानवीय करूणा और भारतीय मनीषा के अनेकानेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन करने वाले इस महामानव ने ४८ वर्षो के छोटे से जीवन में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विधाओं में रचनाएं लिख कर हिंदी साहित्य जगत को सवांर सजाया । १४ जनवरी १९३७ को वाराणसी में निधन, हिंदी साहित्याकास में एक अपूर्णीय क्षति । प्रसाद जी ने अपने नाटकों के माध्यम से भारतीय इतिहास के गौरवपूर्ण चरित्रों को सामने लाते रहे। ’चन्द्रगुप्त’ इनका ऐसा ही एक नाटक है। इस नाटक में भी इन्होंने अपने स्वाभावानुसार सुंदर गीतों का समावेश किया है। इन्हीं में से एक गीत ’हिमाद्रि तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती’ में वे बड़े सुंदर और ओजस्वी ढंग से भारत के वीरों का आह्वान करते हैं।
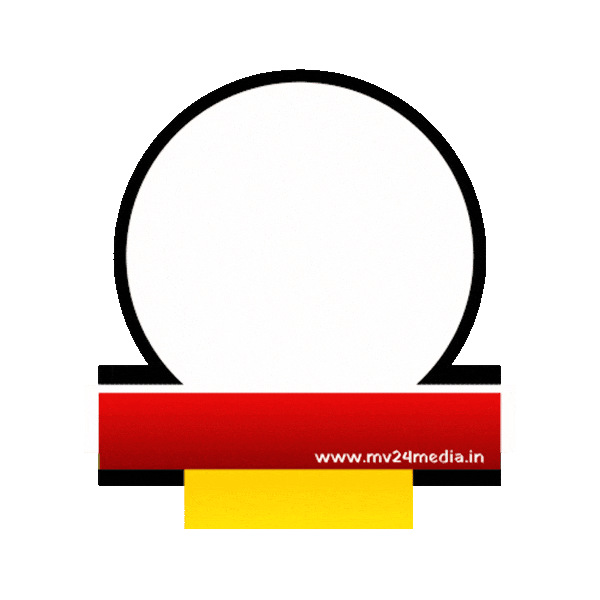
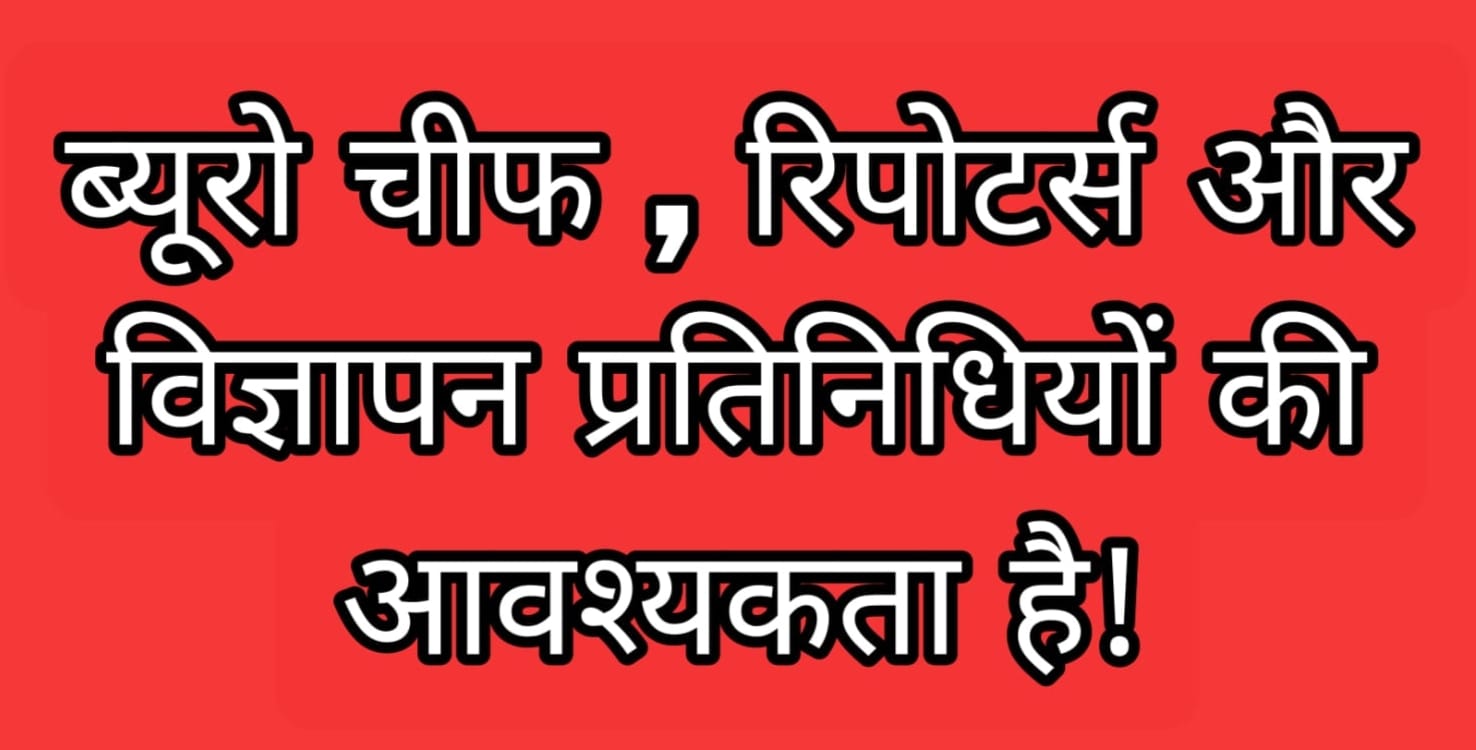
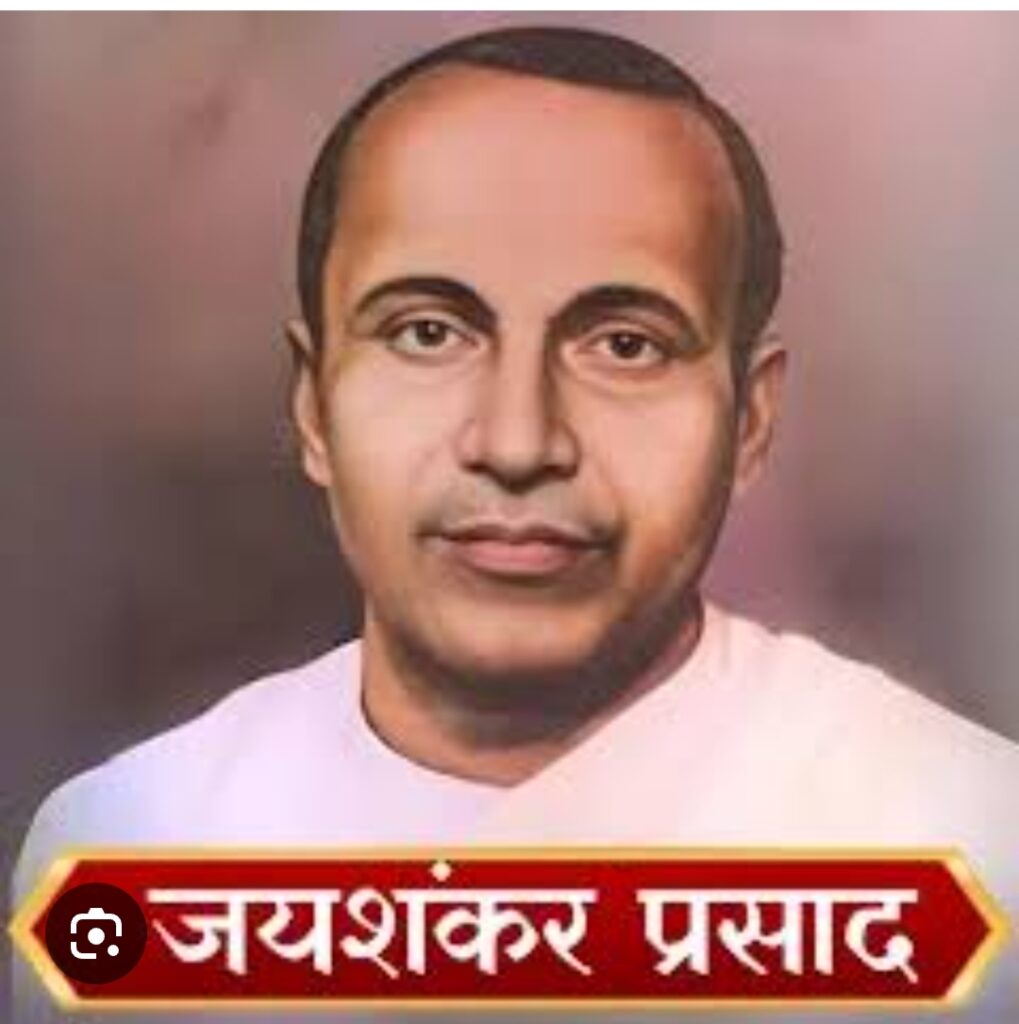








 Users Today : 71
Users Today : 71